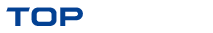ढेला
-क्या नाम है तुम्हारा?
-ढेला
-कहां रहती हो?
– नहीं पहचान रहे हो मुझे?
-पहचानता तो क्यों पूछता?
-यहीं तो रहती हूं, कृपा की लड़की हूं।
-अच्छा, अच्छा…, सुखवंतीन से छोटी हो? तुम्हें तो पहचान नहीं पाया। कितनी बड़ी हो गई हो। तुम्हारी शादी किस गांव में हुई?
– बानबरद ससुराल है मेरा।
-कब से आई हो यहां?
-तीजा पोरा के समय
-तभी से यहीं हो, नहीं गई?
– वो लेने आए तभी न।
– वो लेने आएगा तभी जाओगी, अपने मन से नहीं जाओगी?
-कितनी बार तो अपने मन से जा चुकी हूं, इसके पहले साल भी गई थी।
-तब इस साल क्यों नहीं जाओगी?
-क्या कहूं। बहुत मारपीट करता है। सास-ससुर, देनर-ननद सभी दुख पहुंचाते हैं।
-क्यों?
-मत पूछो भइया…। उन लोगों के बारे में। मेरी एक सौत है। जब उसकी गोद हरी नहीं हुई तो मुझसे शादी कर ले गया था। अब मेरे तीन बच्चे हैं। भगवान की इच्छा भी विचित्र है। इसी बीच सौत के भी बच्चे हुए। उसके भी एक लड़का व एक लड़की है। बस यहीं से मेरी तकदीर फूटी। तब से मेरे साथ मारपीट गालीगलौज शुरू हो गया। रात-दिन सभी ने दुख देते हैं। कितना सहूं…। बहुत दिन तक सहती रही जब नहीं बर्दाश्त कर पाई तो जीता-पोरा में आ गई, तब से नहीं गई।
ढेला अपने बारे में धीरे-धीरे सब कुछ बता गई।
-दामाद क्या करता है? मैंने उससे पूछा।
-खदान में काम करता है।
-खेती-वेती नहीं है?
-बस नाममात्र की है।
– उसे जितना मिलता है गुजर-बसर हो जाती है।
-बस, किसी तरह जिंदगी चल रही है।
– फिर अब क्या हो गया?
-मुझसे अब उसका जी उकता गया है, अपने पास नहीं रखना चाहता। तभी तो ये सब नाटक कर रहा है।
-तब, उससे पूछकर एक बार में ही फैसला नहीं कर लेती?
– उससे क्या पूछूं। सब उसी का किया धरा है।
-तब क्या पंचायत बुलाओगी? अपने समाज के पास जाओगी?
– क्या पंचायत, क्या समाज? गरीब का न पंचायत होता है, न समाज। सब पैसेवालों का है। जब उसका मन ही नहीं है मुझे रखने का, तब पंचायत और समाज क्या कर सकते हैं। बस, मेरे दोनों हाथ पैर सलामत रहें। यहीं मेहनत-मजदूरी कर रह लूंगी,पर वहां मरने के लिए नहीं जाऊंगी।
– तू कैसे समझ बैठी है कि वे तुझे मार डालेंगे?
– पिंजरे में बंद पंछी ही मेरा मन समझ सकता है। किस तरह अत्याचारों को बर्दाश्त करते आई हूं। ….. पिंजरे में बंद रहकर दूसरों के भरोसे रहने की अपेक्षा बाहर रहकर जीना च्छा है।
– अभी तुम्हारी उमर ही कितनी है जो ऐसा कदम उठा रही हो? कहीं बाद में पछताना न पड़े? समझ रही हो न बेटी?
– अब जो होना होगा, होगा। पर उस बेर्रा का मुंह नहीं देखना चाहती।
-अरे ऐसा भी कोई अपने पति को कहता है। जिसने तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा जिसने चुड़ी पहनाई, जिसका नाम लेकर तुम पैरों में महावर रचाती हो उसी को बेर्रा कहती हो?
– अब वो मेरा क्या, मैं कौन उसकी। मेरे लिए तो वह मर गया। मैं जिस दिन यहां आई थी उसने छुरी निकाल कर गला काटने लगा था कि उसी समय सौत ने आकर मुझे बचा लिया। नहीं तो मैं उसी दिन मर गई होती।
इतना सब बताते-बताते ढेला की आंखों से आंसू निकल पड़े।
वह कहने लगी- भैया, मेरा नाम ढेला है। जिस तरह मिट्टी का ढेला हल्की सी चोट में टूटकर, बिखरकर इधर-उधर फैल जाता है उसी तरह मैं हो गई हूं। मैं कब किधर चल दूंगी कोई ठिकाना नहीं। नारी का जीवन ही ऐसा है भइया…। जब एक बार गिरी तो ठोकर खाते हुए बीत जाता है उसे फिर कहीं भी कोई सहारा नहीं मिलता।
– डॉ. निर्मल साहू
(परमानंद वर्मा की छत्तीसगढ़ी कहानी ढेला का हिंदी अनुवाद)